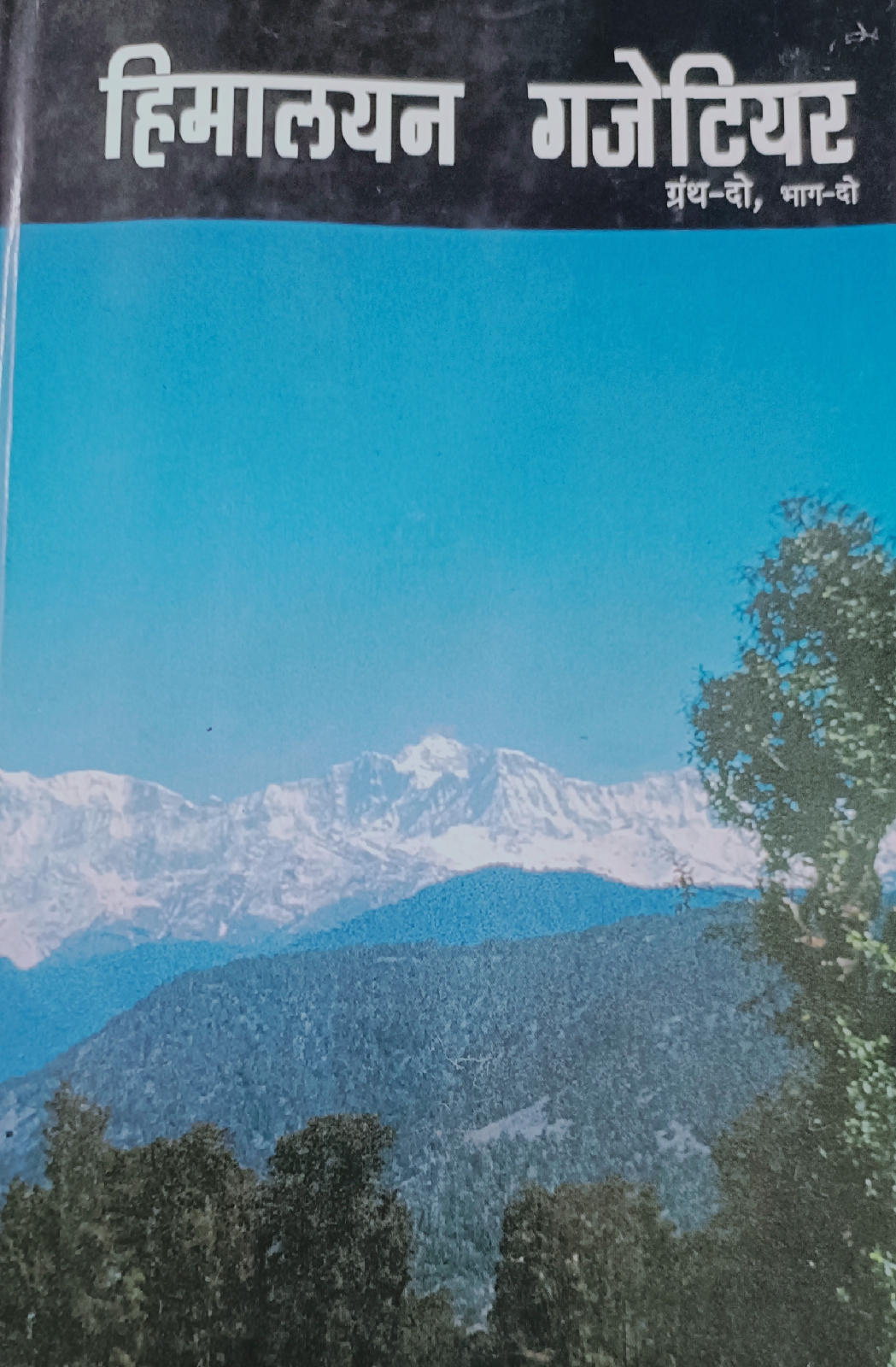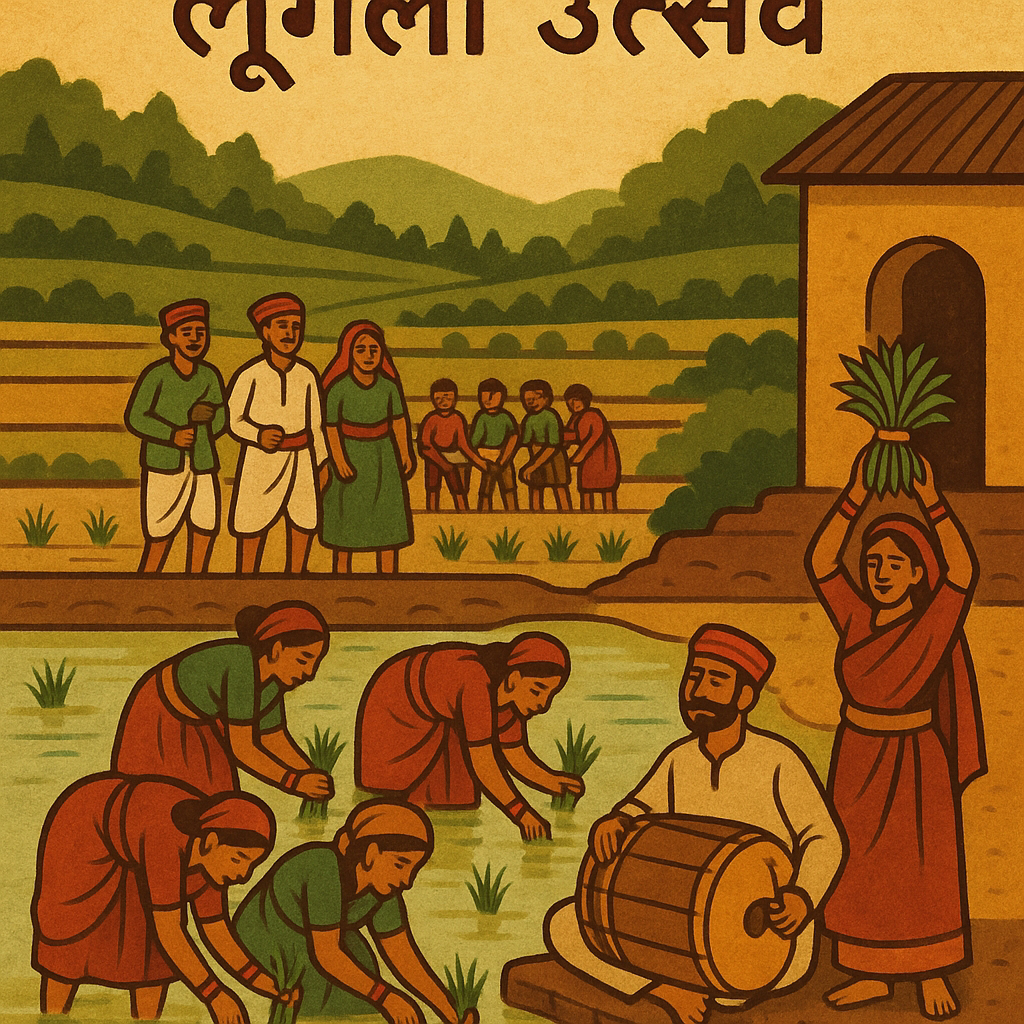उत्तराखंड की प्रमुख लोक देवियाँ

चम्पी/चम्पावतीदेवी: चम्पावत के पुरातन शासकों के द्वारा अपनी कुलदेवी/इष्टदेवी के रूप में पूजित चम्पादेवी का देवालय चम्पावत के मुख्यालय में वहां के प्रसिद्ध देवालय बालेश्वर के पीछे स्थित है। झूमादेवी : स्थानीय लोगों द्वारा इष्टदेवी के रूप में पूजित झूमादेवी का देवस्थल चम्पावत जनपद में लोहाघाट से 4-5 किमी० ऊपर की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। हिंगला : हिडिम्बा के हिंगोले (झूले) से सम्बन्ध वहां के लोगों के द्वारा पूजित यह देवस्थल चम्पावत मुख्यालय से 4 कि०मी० में वनाच्छादित पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। खिलपतिदेवी: खिलपतिदेवी के नाम से स्थानीय लोगों द्वारा पूजित अखिलतारिणीदेवी का यह देवस्थल चम्पावत मुख्यालय से 12-13 कि०मी० उत्तर में खिलपति नामक स्थान में स्थापित है। कोटवीदेवी : यह चम्पावत के मुख्यालय से उत्तर-पश्चिम में स्थित सुंई-बिसुंग के लोगों की इष्टदेवी का स्थान कोटालगढ़ है। यहां के पुरातन शासक असुरराज वाणासुर की माता के रूप में इसकी मान्यता के कारण इसका सम्बन्ध आर्येत्तर वर्गीय देवियों से बनता है। हिडिम्बा हिडिम्ब राक्षस की बहिन होने से हिडिम्बादेवी का सम्बन्ध आयेंत्तर जाति राक्...